*टीवी चैनलों की पत्रकारिता ?*
– *डॉ शाहिद अली*
(वायरलेस न्यूज़ नेटवर्क)
भारत में टीवी चैनलों का विस्तार तेजी से हुआ है। टीवी चैनलों की बाढ़ सी है। शुरुआती दौर में दर्शकों ने दूरदर्शन से टीवी देखने का लुत्फ़ उठाया। दूरदर्शन ने लंबे समय तक दर्शकों को बांधे रखा और सूचना के साथ ही साथ स्वस्थ मनोरंजन के मानक भी गढ़े। भाषा, साहित्य और संस्कृति के स्तर पर दूरदर्शन ने लोगों को ख़ासा आकर्षित किया। प्रिंट मीडिया में चिंता बढ़ी कि कहीं छोटे पर्दे पर प्रसारित समाचारों और मनोरंजन के कार्यक्रमों के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ लेकिन प्रायवेट टीवी चैनलों की बाढ़ और उसमें चलने वाली बहसों में पत्रकारिता में मूल्यों का संकट खड़ा हो गया।
इक्कीसवीं सदी में बुजुर्ग होती पीढ़ी दूरदर्शन के पुराने दिनों को याद करते नहीं थकती। लेकिन वो इस बात से चिंतित नजर आती है कि टीवी चैनलों के नए दौर में पत्रकारिता का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। टीवी में प्रसारित खबरें और एंकरिंग के आक्रामक रवैये व चीख चिल्लाहट ने टीवी के संवाद का स्वाद बदल दिया। टीवी ने ड्राइंग रूम को वार रूम में बदल दिया। टीवी स्टूडियो में ही वार रूम बन गया।
एंकर और बहस में शामिल एक्सपर्ट चैनलों पर जिस तरह हो हल्ला मचाते हैं और जिस तरह बिना किसी नतीजे के बहसें खत्म हो जाती है उससे ये लगता है कि जैसे दर्शकों के ब्लडप्रेशर और धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है। मीडिया के शोधकर्ता इस पर ईमानदारी से अध्ययन करें तो सच्चाई सामने आ सकती है कि टीवी चैनलों की बहसें दर्शकों के लिए कितनी फायदेमंद हैं या दर्शकों में व्यर्थ की उत्तेजना बढ़ाने का माध्यम भर है।
अचरज की बात है कि एक ही एंकर सारे विषयों का जानकार बन जाता है और विशेषज्ञों से सवाल पूछता है। आज देश भर में मीडिया के अनगिनत संस्थान और तीन बड़े पत्रकारिता के विश्वविद्यालय चल रहे हैं। माना जा सकता है कि इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले शिक्षित-प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या भी सैंकड़ों में होगी। ऐसे संस्थानों पर सरकार का एक बड़ा कोष खर्च होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पाठ्यक्रम संस्थानों में पढ़ाए जा रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से इसका लाभ टीवी चैनलों में विविध मुद्दों पर चलने वाली बहस में एक्सपर्ट एंकर के बतौर लिया जाना चाहिए। इससे मीडिया संस्थानों से डिग्री लेकर निकलने वाली युवा पीढ़ी को भी अच्छा करने का अवसर मिलेगा। ये समय घिसी-पिटी व्यवस्था के बोझ लेकर चलने का नहीं है। तकनीक का करिश्मा तो हमने देख ही लिया है। अब एआई का युग है। इसलिए मीडिया संस्थानों के गुरूओं को भी अपने सालों पुरानी पत्रकारिता की शिक्षण कला में बदलाव लाने पर जोर देना होगा।
नई शिक्षा नीति शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच की खाई को खत्म करके एक सेतु बनाना चाहती है। मीडिया संस्थानों और मीडिया उद्योगों को एक दूसरे का मित्र बनना पड़ेगा। समाचार पत्र-पत्रिकाओं, यूट्यूब और टीवी चैनलों के संपादकों को मीडिया के शैक्षणिक संस्थानों का एक जरूरी हिस्सा बनना पड़ेगा। अकादमिक और पेशेवर पत्रकारिता के बीच निरंतर संवाद तय करना होगा। मीडिया संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के निर्माताओं से संवाद का निश्चित कार्यक्रम बनाने की जरूरत है।
पत्रकारिता हमेशा से गंभीर सवालों का समाधान रही है। सवाल करना और उसका सटीक जवाब देना पत्रकारिता को चौथी पालिका का सजग पहरेदार बनाती है। ये संतोष करने का विषय है कि तमाम संकटों के बावजूद प्रिंट मीडिया का सम्मान कम नहीं हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों को कठोर आलोचनाएं सहनी पड़ रही है। टीवी चैनलों की पत्रकारिता कटघरे में खड़ी है। टीवी चैनलों की खबरें विवादों को काफी हद तक बढ़ाने में अपनी सफलता मानती है। खबरों को ब्रेक करने की होड़ में कई बार विश्वसनीयता का संकट खड़ा होता है। यहां तक कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सद्भावना को भी संकट में डाल देते हैं। बड़बोले नेताओं के विवादास्पद बयानों को उछालकर दर्शकों की अच्छी खासी उर्जा और उसकी सोच को भी प्रभावित करने से नहीं चूकते हैं।
यह नहीं भूलना चाहिए कि युवा राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का एक बड़ा तबका टीवी चैनलों की ओर उत्साहित और आकर्षित है। युवाओं की ये पीढ़ी डिजिटल प्रतिभा से लैस है। मीडिया के लिए जरूरी भाषा संपन्न भी है। इनकी योग्यता पर संशय नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें सस्ते में उपलब्ध होने वाला दिहाड़ी समझना चाहिए। इनकी योग्यता और अध्ययन का पूरा सम्मान होना चाहिए क्योंकि टीवी चैनलों की पत्रकारिता पर उठ रहे सवालों और संकटों का जवाब इनके पास है। इन्हें हम उपेक्षित ना करें। टीवी चैनलों की ज़रूरत आज ऐसे प्रतिभा संपन्न मानव संसाधनों की है।
मीडिया संस्थानों से निकलने वाली इन युवाओं की शक्ति से टीवी चैनलों का चेहरा बदल सकता है। दूरदर्शन के युग को दोहराया जा सकता है। यह भी कि दूरदर्शन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने की भी जरूरत है। दूरदर्शन की उपयोगिता को भी नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है। टीवी चैनलों की पत्रकारिता राष्ट्रीय जन-जागरूकता और जन सरोकारों का जरूरी अंग है इसलिए आलोचनाओं से आगे नवाचारों की ओर हमें अग्रसर होना होगा।
( *लेखक सुप्रसिद्ध मीडिया शिक्षाविद् हैं* )
drshahidaliktujm@gmail.com
18/05/2025
Author Profile
Latest entries
 छत्तीसगढ़2025.10.14क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर कन्वेंशन में जिंदल स्टील की टीम ने जीता गोल्ड अवार्ड
छत्तीसगढ़2025.10.14क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर कन्वेंशन में जिंदल स्टील की टीम ने जीता गोल्ड अवार्ड Uncategorized2025.10.14स्पर्श खंडेलवाल बने स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट के चैंपियन- जीती ट्रॉफी और 31 हजार रु.,दुर्ग के वी विराट अय्यर बने उपविजेता, तीसरे स्थान पर रहे बिलासपुर के संकल्प कश्यप
Uncategorized2025.10.14स्पर्श खंडेलवाल बने स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट के चैंपियन- जीती ट्रॉफी और 31 हजार रु.,दुर्ग के वी विराट अय्यर बने उपविजेता, तीसरे स्थान पर रहे बिलासपुर के संकल्प कश्यप Uncategorized2025.10.14अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता मेले में छत्तीसगढ़ी राजभाषा परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन एवं संस्कृति को प्रचारित करने वाले शीतल प्रसाद पाटनवार का सम्मान
Uncategorized2025.10.14अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता मेले में छत्तीसगढ़ी राजभाषा परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन एवं संस्कृति को प्रचारित करने वाले शीतल प्रसाद पाटनवार का सम्मान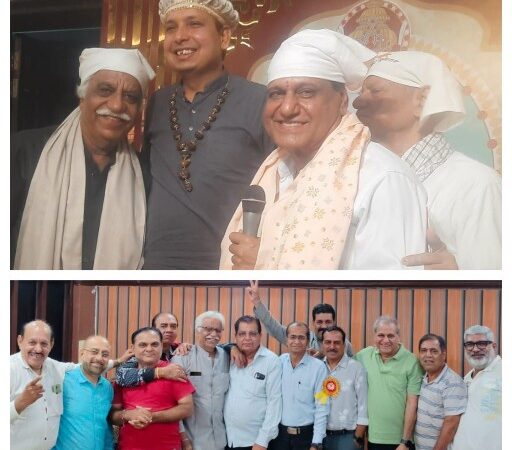 Uncategorized2025.10.14सिंधु कल्चरल एलायंस फोरम का आयोजन: सामूहिक जनेऊ संस्कार में अति विशिष्ट अतिथि होंगे सांई लाल दास
Uncategorized2025.10.14सिंधु कल्चरल एलायंस फोरम का आयोजन: सामूहिक जनेऊ संस्कार में अति विशिष्ट अतिथि होंगे सांई लाल दास



